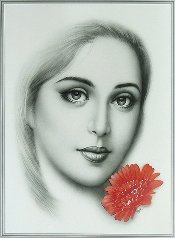अंधेरे के अज्ञान पर
मुस्कुरा उठी
मन में बाती
पूछ्ते हो
जिस वज़ूद के
फ़ना होने का मकसद
जन्मा है वो बस
जलने के लिए
रूप यौवन
सब है व्यर्थ
काम ना आऊं गर
ज़माने के लिए
तम को मिटाना
नहीं मंज़िले-मक़सूद मेरी
वक़्त-ए-ज़रूरत
रोशन कर आलम को
जीना है फ़ितरत मेरी
जिसे तुम कहते
जल जल मरी
वही तो
लुत्फ़-ए-ज़िंदगानी है
किसी घर को करा
मैने रोशन,वही
मेरी राहते रूहानी है
मोहब्बत खुद से है इतनी
फ़ना होती
हूँ अपने लिए
ना जलूं मैं गर
तो बेकार हैं
तेल भरे दिए
वो मेरे हमसफर
देते हैं साथ मेरा
मंज़िल को पाने में
तुम विराट होके भी
दुबक जाते हो
पनाह में दिए की
जिस लम्हा जलती
मैं ज़माने में
ना कोशिश करो
भरमाने की मुझको
एहसास है मुझे
दोस्ती का अपनी
दिए व तेल के साथ
वफ़ा और जफ़ा का
कोई बंधन नहीं
बस जीते हैं
लिए हाथों में हाथ
रहे भटकाते तुम
सभी को ,
राह दिखाती मैं हूँ
नहीं हटूँगी पथ से अपने
मैं इसी जलने में
खुश हूँ मगन हू
बिन दीपक बाती अधूरी
बाती बिना दिया भी हारा
भीग दिए के प्रेम तेल में
रोशन करते ये जग सारा
रविवार, 24 मई 2009
betabi
कैसा सरूर है ये,कैसी है बेताबी
दस्तक होने से पहले दिल धड़क उठता है
और उठ जाती हूँ मैं खोलने दर को
दूर तक घूम के नज़रें फिर
लौट आती हैं दीवार पर लगी घड़ी की तरफ
जो बिना किसी बेताबी के अपने नियमों में बंधी
सुकून से चलती रहती है....
क्यूँ मैं इस घड़ी की तरह
वक़्त से बेपरवाह हो कर नहीं चल सकती
क्यूँ जीवंत पलों को वक़्त की सीमाओं में बांधा है मैंने..
ये बेताबी ये बेचैनी सब स्वतः ही घुल जायेंगे
जीने लगूं गर मैं पल दर पल...
घड़ी के सेकेंड के कांटे की तरह .....
दस्तक होने से पहले दिल धड़क उठता है
और उठ जाती हूँ मैं खोलने दर को
दूर तक घूम के नज़रें फिर
लौट आती हैं दीवार पर लगी घड़ी की तरफ
जो बिना किसी बेताबी के अपने नियमों में बंधी
सुकून से चलती रहती है....
क्यूँ मैं इस घड़ी की तरह
वक़्त से बेपरवाह हो कर नहीं चल सकती
क्यूँ जीवंत पलों को वक़्त की सीमाओं में बांधा है मैंने..
ये बेताबी ये बेचैनी सब स्वतः ही घुल जायेंगे
जीने लगूं गर मैं पल दर पल...
घड़ी के सेकेंड के कांटे की तरह .....
मुख्तसर सा लम्हा
अनजान राहों पे खड़ी
देख रही हूँ कारवाँ
लम्हों का
कुछ नन्हे मुन्ने
कुछ अल्हड़
कुछ परिपक्व
और कुछ बुजुर्ग से
हर लम्हा अपने में पूर्ण
देख कर सोचती हूँ
कौन सा है वो
मुख्तसर सा लम्हा
जो छम से आ गिरेगा
मेरी गोद में
और खिल जाऊंगी मैं
उस एक लम्हे के
अपना होने के एहसास से
पालूंगी पोसूँगी
जी लूँगी उसके बचपन में
अपना बचपन
फिर यौवन उस लम्हे का
भिगो देगा मेरा तन मन
और फिर होगा वो परिपक्व
सिखाता हुआ मुझे
बाहर आना इन
मेरे तेरे के भावों से
क्यूँ जी नहीं लेती मैं
उन सब लम्हों को
जो गुज़र रहे हैं
हंसते मुस्कुराते हुए
मेरी नज़रों के आगे से...
उस एक मुख्तसर से लम्हे
के इंतेज़ार में
बिछुड़ जाती हूँ
उस कारवाँ से
जिसकी राह भी मैं
और शायद
मंज़िल भी मैं....
देख रही हूँ कारवाँ
लम्हों का
कुछ नन्हे मुन्ने
कुछ अल्हड़
कुछ परिपक्व
और कुछ बुजुर्ग से
हर लम्हा अपने में पूर्ण
देख कर सोचती हूँ
कौन सा है वो
मुख्तसर सा लम्हा
जो छम से आ गिरेगा
मेरी गोद में
और खिल जाऊंगी मैं
उस एक लम्हे के
अपना होने के एहसास से
पालूंगी पोसूँगी
जी लूँगी उसके बचपन में
अपना बचपन
फिर यौवन उस लम्हे का
भिगो देगा मेरा तन मन
और फिर होगा वो परिपक्व
सिखाता हुआ मुझे
बाहर आना इन
मेरे तेरे के भावों से
क्यूँ जी नहीं लेती मैं
उन सब लम्हों को
जो गुज़र रहे हैं
हंसते मुस्कुराते हुए
मेरी नज़रों के आगे से...
उस एक मुख्तसर से लम्हे
के इंतेज़ार में
बिछुड़ जाती हूँ
उस कारवाँ से
जिसकी राह भी मैं
और शायद
मंज़िल भी मैं....
रिश्तों के रखाव में ......
रिश्तों के
रखाव में
सहजता का
अभाव क्यूँ...?
सुना था
बचपन से
नर-नारी
आपस में
दोस्त कभी
हो नहीं सकते
बिना किसी
नियत नाम के
समाज में
विचरण
कर नहीं सकते
स्त्री के हैं
नियमित रिश्ते
पिता, भाई,
पति और बेटा
इनसे पृथक
कोई भी रिश्ता
उसको
इज़्ज़त
नहीं है देता
सती कहा जाता
द्रौपदी को
हुए मित्र
सबसे अच्छे
जिसके
स्वयं पालनहार
धरा के
किसुन-कन्हाई
संग थे उसके
पांचाली को
कहते कृष्णा भी
कृष्ण की
अभिन्न सखी
थी वो...
हर उस लम्हा
बने थे संबल
खाविन्दो के झुंड
में भी
जब होती अकेली
थी वो ....
कौरवों की
घृणित चौकड़ी में
हारे थे जब
पाँचों पांडव
मर्दों के उस
लोलुप ज़ज़्बे का
कैसा घटित
हुआ था तांडव
द्रौपदी को
लगा दाँव पे
नैन झुकाए
बैठे थे सब
लाज बचाई
मित्र ने उसकी
करुंण हृदय
चीत्कार उठा जब
नहीं लांच्छित
हुआ वो रिश्ता
नहीं मापदंड था
उसका कोई
फिर क्यूँ सब
डरे से रहते
नाम ढूँढ कर
देते कोई
समाज की
संकीर्ण सोचों में
वह महासती
कहाँ है खोई
कृष्ण के
हर रिश्ते के
कुदरती होने के
एहसास का..
नहीं समाज पर
प्रभाव क्यूँ???
रिश्तों के
रखाव में
सहजता का
अभाव क्यूँ...?
रखाव में
सहजता का
अभाव क्यूँ...?
सुना था
बचपन से
नर-नारी
आपस में
दोस्त कभी
हो नहीं सकते
बिना किसी
नियत नाम के
समाज में
विचरण
कर नहीं सकते
स्त्री के हैं
नियमित रिश्ते
पिता, भाई,
पति और बेटा
इनसे पृथक
कोई भी रिश्ता
उसको
इज़्ज़त
नहीं है देता
सती कहा जाता
द्रौपदी को
हुए मित्र
सबसे अच्छे
जिसके
स्वयं पालनहार
धरा के
किसुन-कन्हाई
संग थे उसके
पांचाली को
कहते कृष्णा भी
कृष्ण की
अभिन्न सखी
थी वो...
हर उस लम्हा
बने थे संबल
खाविन्दो के झुंड
में भी
जब होती अकेली
थी वो ....
कौरवों की
घृणित चौकड़ी में
हारे थे जब
पाँचों पांडव
मर्दों के उस
लोलुप ज़ज़्बे का
कैसा घटित
हुआ था तांडव
द्रौपदी को
लगा दाँव पे
नैन झुकाए
बैठे थे सब
लाज बचाई
मित्र ने उसकी
करुंण हृदय
चीत्कार उठा जब
नहीं लांच्छित
हुआ वो रिश्ता
नहीं मापदंड था
उसका कोई
फिर क्यूँ सब
डरे से रहते
नाम ढूँढ कर
देते कोई
समाज की
संकीर्ण सोचों में
वह महासती
कहाँ है खोई
कृष्ण के
हर रिश्ते के
कुदरती होने के
एहसास का..
नहीं समाज पर
प्रभाव क्यूँ???
रिश्तों के
रखाव में
सहजता का
अभाव क्यूँ...?
सुनी पहाड़ ने पुकार ज़मीन की.....
सुनी पहाड़ ने पुकार ज़मीन की...
हर लम्हा उसकी हम-नशीन की
चकरा गया वो सुन के ये बातें
अपने गुरूर पे की गयी घाते
हैरान सा देखता रहा ज़मीन को
समझा था हमसाया उस हसीन को
आज वही उसको समझ ना पाई है
उसकी दृढ़ता उसे अकड़ नज़र आई है
ना सहता मैं कड़कड़ाती बिजलियाँ
तो जल गयी होती तू कभी की
तुझ से पहले घात सह कर हवा का
जान बचती है तुझपे बसने वालो सभी की
गम नहीं बदन के घुलने का मुझे
मिल के बन जाता है हस्ती वो भी ज़मीन की
और बनती है धरा फिर और सुंदर
खुश्बू होती है हवा में तेरी नमी की
एक होने का सुकून मिलता है मुझको
तूने कैसे सोचा जज़्बा-ए-गुरूर है
हूँ जुड़ा गहरा जड़ों तक मैं जो तुझसे
मेरे जीने का तो ये दिलकश सुरूर है
सूरज का ताप औ बर्फ़ीली हवायें
तुझको झुलसा ना दें ठिठूरा ना जायें
इस वजह खड़ा हूँ यूँ सीना तान कर मैं
तेरे कोमल मन को ये चटका ना जायें
आज तूने यूँ पुकारा ए हम-नशीन
बात कुछ अनकही तुझ तक पहुँची नही
तू है तो मैं हूँ,मैं हूँ तो तू है
कहाँ इसमें अकड़ और कहाँ इसमें गुरूर है
मैं हूँ जाहिल और तू ज़हीन है
इसीलिए ये रिश्ता पूरक है , हसीन है
चल साफ कर मेरे लिए तू मन ये अपना
आ मिल कर देखे सुन्दर धरा का हम सपना
हर लम्हा उसकी हम-नशीन की
चकरा गया वो सुन के ये बातें
अपने गुरूर पे की गयी घाते
हैरान सा देखता रहा ज़मीन को
समझा था हमसाया उस हसीन को
आज वही उसको समझ ना पाई है
उसकी दृढ़ता उसे अकड़ नज़र आई है
ना सहता मैं कड़कड़ाती बिजलियाँ
तो जल गयी होती तू कभी की
तुझ से पहले घात सह कर हवा का
जान बचती है तुझपे बसने वालो सभी की
गम नहीं बदन के घुलने का मुझे
मिल के बन जाता है हस्ती वो भी ज़मीन की
और बनती है धरा फिर और सुंदर
खुश्बू होती है हवा में तेरी नमी की
एक होने का सुकून मिलता है मुझको
तूने कैसे सोचा जज़्बा-ए-गुरूर है
हूँ जुड़ा गहरा जड़ों तक मैं जो तुझसे
मेरे जीने का तो ये दिलकश सुरूर है
सूरज का ताप औ बर्फ़ीली हवायें
तुझको झुलसा ना दें ठिठूरा ना जायें
इस वजह खड़ा हूँ यूँ सीना तान कर मैं
तेरे कोमल मन को ये चटका ना जायें
आज तूने यूँ पुकारा ए हम-नशीन
बात कुछ अनकही तुझ तक पहुँची नही
तू है तो मैं हूँ,मैं हूँ तो तू है
कहाँ इसमें अकड़ और कहाँ इसमें गुरूर है
मैं हूँ जाहिल और तू ज़हीन है
इसीलिए ये रिश्ता पूरक है , हसीन है
चल साफ कर मेरे लिए तू मन ये अपना
आ मिल कर देखे सुन्दर धरा का हम सपना
नज़रों में ज़माने की
लबों पे मेरे जब मस्सर्त-ए-जज़्बात उतर आए
नज़रों में ज़माने की सवालात उभर आए
रहे ग़मज़दा तो सुकून से रहती है ये दुनिया
अंधेरों से ना आओ उजाले में ,कहती है ये दुनिया
क्यूँ गुनगुना उठा दिल क्यूँ चमक गयी आँखें
क्या हुआ जो तब्बस्सुम-ए-रुखसार निखर आए..
नज़रों में........
किस का करे गिला ये दिल ,किस को पुकारे
हर शख्स परीशां है खुद अपने ज़हन में
खुशियों का ख़जाना है हर इक को मयस्सर
झाँको ज़रा खुद में तो हालात सुधर जाए
नज़रों में ज़माने की.....
नज़रों में ज़माने की सवालात उभर आए
रहे ग़मज़दा तो सुकून से रहती है ये दुनिया
अंधेरों से ना आओ उजाले में ,कहती है ये दुनिया
क्यूँ गुनगुना उठा दिल क्यूँ चमक गयी आँखें
क्या हुआ जो तब्बस्सुम-ए-रुखसार निखर आए..
नज़रों में........
किस का करे गिला ये दिल ,किस को पुकारे
हर शख्स परीशां है खुद अपने ज़हन में
खुशियों का ख़जाना है हर इक को मयस्सर
झाँको ज़रा खुद में तो हालात सुधर जाए
नज़रों में ज़माने की.....
खुद को
नज़र रही मशरे पर ना अपनाया खुद को
इसी जद्दो-ज़हद में बिसराया खुद को
खुश रखने की चाहत में हर गैरोसनम को
निगाहों से कई बार गिराया खुद को
नज़र पड़ी रूह-ए-खुदा पर तो जाना
बेकार ही यहाँ वहाँ ढूँढा किया खुद को
बीते हर लम्हा अब तेरी बंदगी में
पेश्तर तुझे पाने के ,अपनाया खुद को
दरिया-ए-मस्सरत का लुत्फ़ क्या कहिये
डूब के इस धारे में ,बहाया खुद को
ए मेरे मलिक कर दे इस लायक मुझे
बाँट भी पाऊं जो आज पाया खुद को
इसी जद्दो-ज़हद में बिसराया खुद को
खुश रखने की चाहत में हर गैरोसनम को
निगाहों से कई बार गिराया खुद को
नज़र पड़ी रूह-ए-खुदा पर तो जाना
बेकार ही यहाँ वहाँ ढूँढा किया खुद को
बीते हर लम्हा अब तेरी बंदगी में
पेश्तर तुझे पाने के ,अपनाया खुद को
दरिया-ए-मस्सरत का लुत्फ़ क्या कहिये
डूब के इस धारे में ,बहाया खुद को
ए मेरे मलिक कर दे इस लायक मुझे
बाँट भी पाऊं जो आज पाया खुद को
बंजर धरा
बंजर सी धरती पे
क्यूँ बरसाए नेह का सावन
कठोर है धरा
बीज तक ना पंहुचेगा तेरा आवाहान
प्रेम के हल से करी जुताई
बीज धरा में तूने बोया
नम अँखियों से सींचा उसको
व्यर्थ प्रतीक्षा में ना सोया
देख धरा पे कुछ त्रिन हैं
स्वतः ही जनम हुआ है उनका
सहज स्वाभाविक अवसर पा कर
उदगम नैसर्गिक हुआ है उनका
ना शोक मना तू बांझ धरा का
तूने करम किया स्व पूरा
जितना मिलना लिखा भाग्य में
वो नहीं मिलेगा कभी अधूरा
ले आनंद उन्ही त्रिनो का
कन कन प्रतिकन ही तो जीवन है
हर क्षण को सींच प्रेम अँसुअन से
यही मनुष्य सार्थक जीवन है
क्यूँ बरसाए नेह का सावन
कठोर है धरा
बीज तक ना पंहुचेगा तेरा आवाहान
प्रेम के हल से करी जुताई
बीज धरा में तूने बोया
नम अँखियों से सींचा उसको
व्यर्थ प्रतीक्षा में ना सोया
देख धरा पे कुछ त्रिन हैं
स्वतः ही जनम हुआ है उनका
सहज स्वाभाविक अवसर पा कर
उदगम नैसर्गिक हुआ है उनका
ना शोक मना तू बांझ धरा का
तूने करम किया स्व पूरा
जितना मिलना लिखा भाग्य में
वो नहीं मिलेगा कभी अधूरा
ले आनंद उन्ही त्रिनो का
कन कन प्रतिकन ही तो जीवन है
हर क्षण को सींच प्रेम अँसुअन से
यही मनुष्य सार्थक जीवन है
गुरुवार, 21 मई 2009
बंद दरवाजे

उसके मकां के बंद "दरवाजे"..
तोड़ देते हैं हिम्मत मेरी
दस्तक देने के लिए..
मकां के दर खुले तो
दस्तक दूँ उसके मन के दरों पर भी..
अपने हर दर को बंद कर
यूँ ज़िन्दगी से गिले करना
आदत सी हो गयी है उसकी..
सहज हवा का झोंका ही
पल्ले हिला दे और उस दस्तक से
वो बढ़ के खोल दे वो बंद दरवाजे
तो शायद मुझे मौका मिले
उसके मन पे दस्तक देने का..
तोड़ देते हैं हिम्मत मेरी
दस्तक देने के लिए..
मकां के दर खुले तो
दस्तक दूँ उसके मन के दरों पर भी..
अपने हर दर को बंद कर
यूँ ज़िन्दगी से गिले करना
आदत सी हो गयी है उसकी..
सहज हवा का झोंका ही
पल्ले हिला दे और उस दस्तक से
वो बढ़ के खोल दे वो बंद दरवाजे
तो शायद मुझे मौका मिले
उसके मन पे दस्तक देने का..
सदस्यता लें
संदेश (Atom)